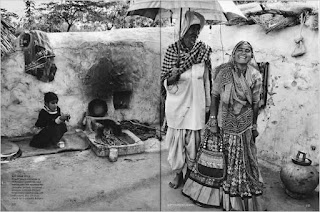सीक्रेट

उस दिन कान में वो सीक्रेट बात कहते हुए उसके कितना करीब आगई थी वो। कितना अलग लग रहा था उसे। पहले कभी वो किसी के इतना करीब नही आई थी। उसने सोचा ही नही था कि वो कभी अपने घर से इस समय बाहर आ भी पाएगी। सात बज रहे थे पर दोनों को घर की ज़रा भी याद नही आ रही थी। ठंड भी तो थी, एक अजीब सी ख़ुश्बू आ रही थी उस ठंडी हवा में घुलकर, उसने कभी नही सूँघा था, उस ख़ुश्बू को। शाम ज़रा और ठहर जाती तो वो उस फूल को भी ढूंढ निकालती। सुबह अपने बालों के छल्ले बनाकर आई थी वो, अब वो छल्ले वो ख़ुद खोल चुकी थी। कब से आज के दिन का इंतज़ार कर रही थी वो पर इतनी जल्दी शाम हो गई। उसका मन हुआ काश वो किसी एक शाम किसी फुटपाथ पर बैठकर यूँ ही उससे बातें करती रहे। वो शाम शायद ही कभी आ पाए। उसे हर शाम क्यों घर लौटना होता है? उसे भले ही महसूस हो रहा हो कि उसे उससे प्यार है पर वो क़ुबूल ही नही कर रही थी, करे भी कैसे? वो कुछ कहता ही नही. बस चुपचाप उसकी चपर-चपर सुनता रहता है। कितना..? डेढ़ साल तो हो गया होगा उनकी दोस्ती को, वो कभी इस क़दर खुलता ही नही की उसको समझा जा सके। कभी-कभी उसे लगने लगता है कि उसकी चपर-चपर की वजह से ही वो बोल